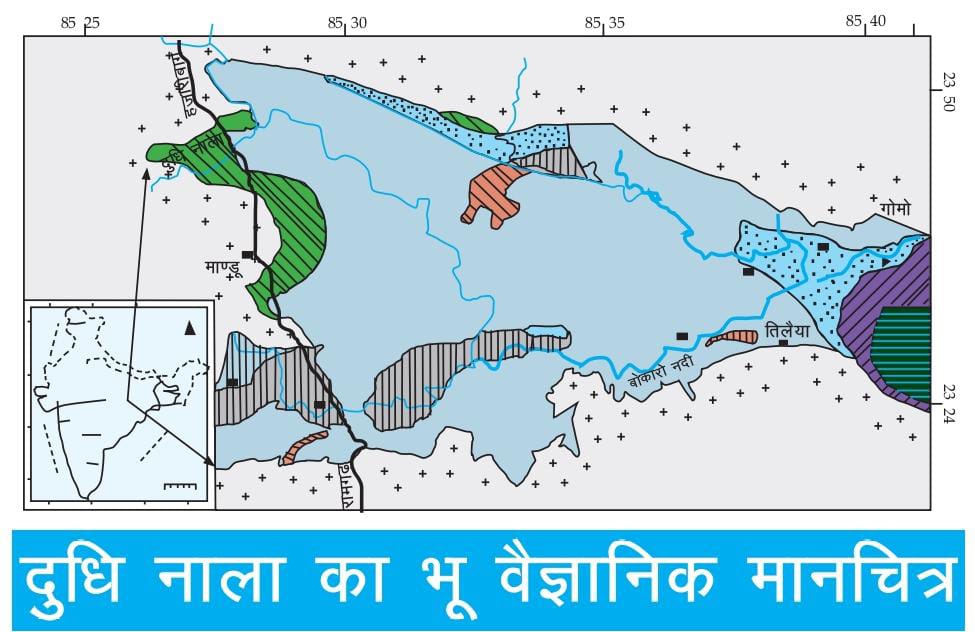प्रमोद भार्गव
अनेक कानूनी उपाय और जागरूकता अभियानों के बावजूद बच्चों से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 60 दिन के भीतर ऐसे जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन करे, जहां बाल यौन उत्पीड़त से जुड़े 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इन अदालतों का गठन बाल यौन उत्पीड़न निषेध कानून (पॉक्सो) के तहत होगा। ये अदालतें सिर्फ पॉक्सो से संबंधित मामले ही सुनेंगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में अदालत ने देशभर से बाल दुष्कर्म के मामलों के आंकड़े इकट्ठे किए थे। इससे पता चला कि एक जनवरी से 30 जून 2019 तक बालक-बालिकाओं से दुष्कर्म के 24,212 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6,449 में ही चालान पेश किया गया। तब जाकर अदालतों में सुनवाई शुरू हुई और 911 में त्वरित निर्णय भी हो गया। इन अदालतों के गठन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। साथ ही अदालत ने बाल यौन उत्पीड़न पर नियंत्रण के लिए एक लघु वीडियो फिल्म बनाने का सुझाव भी दिया है। इसका प्रसारण सिनेमाघरों और टीवी चैनलों पर होगा। चूंकि शीर्ष न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए हैं। इसलिए तय है कि विशेष अदालतों के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अदालतें समानता के धरातल पर बाल दुष्कर्म से जुड़े कितने मामलों में तत्परता से फैसले दे पाती हैं, यह इनके गठन के कुछ समय बाद ही साफ होगा। क्योंकि, ऐसे मामलों में जो गरीब और लाचार आरोपी थे, उन्हें तो कम से कम समय में सजा दे दी गई, लेकिन इसी प्रकृति के मामलों में सक्षम व धनी आरोपियों के विरुद्ध जांच भी पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए 24,000 मामलों में से महज 911 में ही त्वरित न्याय हो पाया है। यदि इस कार्य-संस्कृति से विशेष अदालतें चलेंगी तो सरकार पर बोझ के अलावा इनका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। उपभोक्ता, किशोर और कुटुंब न्यायालयों का भी यही हश्र हुआ है। दुष्कर्म मामलों में त्वरित न्याय का सिलसिला चल निकलने के बाद भी बलिकाओं से रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा और 16 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया था। अब इस आध्यादेश को संसद के इसी सत्र में विधेयक लाकर कानूनी रूप दे दिया गया है। पॉक्सो कानून की धारा 9 के तहत किए गए प्रावधानों में शामिल है कि बच्चों को सेक्स के लिए परिपक्व बनाने के उद्देश्य से उन्हें यदि हार्मोन या कोई रसायनिक पदार्थ दिया जाता है तो इस पदार्थ को देने वाले और उसका भंडारण करने वाले भी अपराध के दायरे में आएंगे। इसी तरह पोर्न सामग्री उपलब्ध कराने वाले को भी दोषी माना गया है। ऐसी सामग्री को न्यायालय में सबूत के रूप में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि अधिकतम मामलों में पुलिस ने कामवर्द्धक दवा और अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। दरअसल, इस तरह की चीजें बच्चों से बाल्यावस्था छीनने का कारण बनते हैं। इनसे प्रेरित होकर किसी स्त्री के साथ अनर्थ होता है तो उसका शरीर ही नहीं अत्मा भी छलनी होती है। हालांकि पहले कानून से कहीं ज्यादा आदमी को धर्म और समाज का भय था। नैतिक मान-मर्यादाएं कायम थीं। किंतु इन्हें तार-तार करने का काम कुछ ऐसे कानूनों ने भी किया है, जिनके चलते रिश्तों की गरिमा लगभग खत्म हो गई है। नैतिक पतन के कई स्वरूप होते हैं, व्यक्तिगत, संस्थागत और सामूहिक। व्यक्तिगत पतन स्वविवेक और पारिवारिक सलाह से रोका जा सकता है। किंतु संस्थागत और सामूहिक चरित्रहीनता के कारोबार को सरकार और पुलिस ही नियंत्रित कर सकती है। दवा कंपनियां कामोत्तेजना बढ़ाने के जो रसायन और सॉफ्टवेयर कंपनियां पोर्न फिल्में बनाकर जिस तरह से इंटरनेट पर परोस रही हैं, उस पर काबू कानूनी उपायों से ही संभव है। पोर्न फिल्मों की ही देन है कि जैसे गली-गली में दुष्कर्मी घूम रहे हैं। समाजशास्त्री मानते हैं कि जहां कानूनी प्रावधानों के साथ सामाजिक दबाव भी होता है, वहां बलात्कार जैसी दुष्प्रवृतियां कम पनपती हैं। बाल उत्पीड़न की ज्यादातर घटनाएं महानागरों के उन इलाकों में घट रही हैं, जहां समाज और परिवार से दूर वंचित समाज रह रहा है। ये लोग अकेले गांव में रह रहे परिवार की आजीविका चलाने के लिए शहर में मजदूरी करने आते हैं। मोबाइल पर उपलब्ध कामोत्तेजक सामग्री इन्हें भड़काने का काम करती है और ये चलती-फिरती बालिकाओं को बहला-फुसलाकर बाल यौन उत्पीड़न कर डालते हैं। चूंकि ये परिवार और रिश्तेदारों से दूर गुमनाम-सी जिंदगी जीते हैं, इसलिए इन्हें यह भरोसा रहता है कि दुष्कर्म के बाद भी उनकी पहचान मुश्किल है। ये लोग चूंकि जागरूक नहीं होते, इसलिए उन्हें कानून का भय भी नहीं होता। ऐसे लोग अपराधमुक्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पत्नी, परिवार और समाज की सामूहिकता उपलब्ध कराई जाए। नैतिक बल के लिए सामाजिक वातावरण इर्दगिर्द होना जरूरी है। देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म में फांसी का कानून वजूद में लाया गया है। बावजूद देश की सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा था कि ‘देश में राइट, लेफ्ट और चहुंओर दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं।’ इतनी कठोर टिप्पणी अदालत को इसलिए करनी पड़ी है, क्योंकि पांच साल की बच्ची से लेकर 75 साल की वृद्धा तक दुष्कर्म के मामले रोजाना खबर बन रहे हैं। अब यह अच्छी बात है कि शासन-प्रशासन और न्यायापालिका इस दृष्टि से सचेत दिख रहे हैं। विशेष अदालतों का गठन इसी चिंता का परिणाम है। दरअसल बच्चियों के साथ हैवानियत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बावजूद न्यायशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि जीवन खत्म करने का अधिकार आसान नहीं होना चाहिए। इसलिए फांसी की सजा जघन्यतम या दुर्लभ मामलों में ही देने की परंपरा है। इसीलिए निचली अदालत से सुनाई गई फांसी की सजा पर अमल भी जल्दी नहीं होता। मप्र में 2018 में 58 दोषियों को दुष्कर्म व हत्या के मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन एक भी सजा पर अमल नहीं हो पाया है। यह मामले उच्च, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के पास दया याचिका के बहाने लंबित हैं। सभी जगह दोषी को क्षमा अथवा सजा कम करने की प्रार्थना से जुड़े आवेदन लगे हुए हैं। इन आवेदनों के निरस्ती के बाद ही दोषी का फांसी के फंदे तक पहुंचना मुमकिन हो पाता है। साफ है, दुष्कर्म से जुड़े कानूनों को कठोर बना दिए जाने के बावजूद इस परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। पुलिस और अदालतों की कार्य-संस्कृति यथावत है। मामले तारीख दर तारीख आगे बढ़ते रहते हैं। कभी गवाह अदालत में पेश नहीं होते हैं तो कभी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आने के कारण तारीख बढ़ती रहती है। इस बाबत न्यायिक व पुलिस कानून में सुधार की बात काफी समय से उठ रही हैं, लेकिन हमारी सरकारों की प्राथमिकता में कानूनी सुधार की चिंता है ही नहीं? लिहाजा विशेष अदालतें गठित हो भी जाएं तो कानूनी प्रक्रिया में शिथिलता होने के कारण गति आना मुश्किल है।
This post has already been read 25901 times!